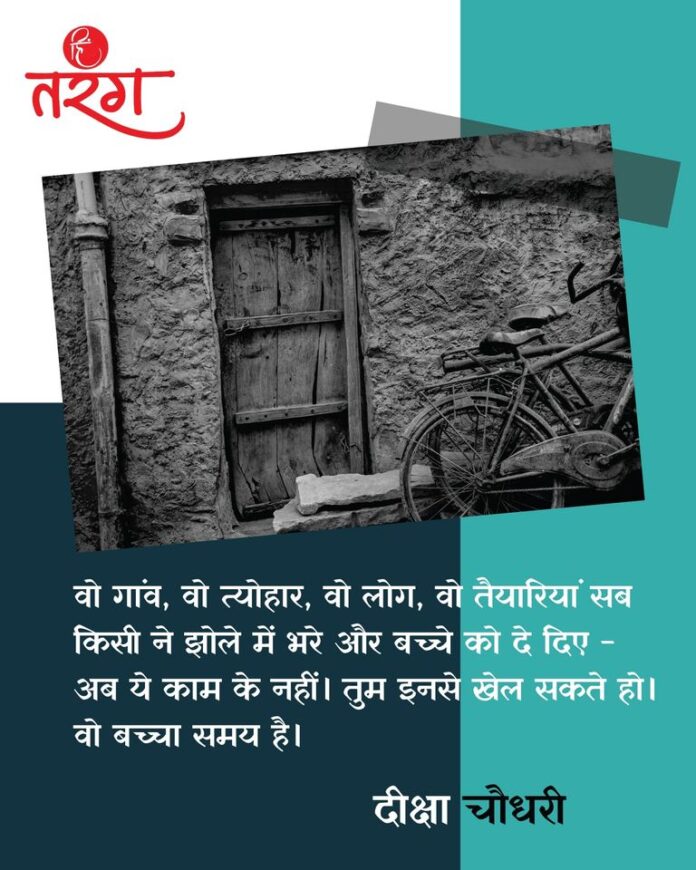आह! दिवाली की तैयारियों के ये दिन! चूने की ख़ुशबू तो नहीं आ रही? देखो! नलके के पास हांडी में चूना भिगोकर रखा है क्या? नहीं? ओह तो स्मृति थी। कैसी तो सुंदर। साझा करने को जी नहीं चाहता। कोई चुरा न ले जाए। स्मृतियों के सिवा कुछ बचा ही कहाँ। नदी में बाढ़ की तरह समय आया, सब बहा ले गया। अब जलकुंभियों की तरह उगी हैं ये स्मृतियाँ। मैं इनकी रखवाली करने बैठी हूँ। एक चित्र याद आ गया। घर की पिछली गली की तरफ़ लम्बी दीवार थी। कच्ची ईंटों से बनी। दिवाली से पहले इन दिनों उसे गोबर से लीपा जाता था। माँ मदद के लिए खेत में काम करने वाले राजू ताऊ की पत्नी को बुला लेती थीं। घर का काम धंधा ख़त्म करने के बाद दोनों दीवार लीपने लगतीं। आसपास के घरों की औरतें भी बारी बारी से वहाँ आती रहतीं। कभी कोई जग में भरकर चाय ले आती। फिर सब वहीं साथ बैठकर पीतीं। कोई बताने लगती कि वो तो अभी पशुओं के ठाण लीप रही है, उसके बात घर के अंदर की सफ़ाई शुरू करेगी। और बस हथाई (बातचीत) शुरू हो जाती। सब अपनी अपनी रणनीति बताने लगते। शायद मिलान करते थे कि वो इस तरह काम करते रहने से दिवाली तक घर की साफ़ सफ़ाई में सफ़ल हो पाएंगी या नहीं। बड़े बड़े घर होते थे। बड़े बड़े बरामदे, आंगन और मालिए (छत पर बना कमरा)।महीने भर पहले काम शुरू होता तब जाकर दिवाली तक पूरा हो पाता। मेरा स्कूल गाँव के दूसरे कोने पर था। आधी छुट्टी खाना खाने घर आती थी। अपने घर की पिछली गली में माँ को देखकर सीधी उन्हीं के पास चली आती। वो बतातीं रोटी सब्जी कहां रखी है, वहाँ से कैसे लेनी है। मैं आगे के दरवाज़े की बजाय वहीं दीवार पर लगी निसरणी पर चढ़कर घर के अंदर पिंकली भैंस के ठाण में कूद जाती। वो भैंस हमेशा मुझे मारने के लिए भागती थी। पर इन दिनों इस समय सारे पशु दूसरे खूंटों पर बंधे होते थे जहां मकानों की छाया ढलती थी। मुझे सीधे दरवाजे की बजाय इस तरह कूदकर घर में जाना बड़ा रोमांचक लगता था। जैसे एक ढर्रे पर चलते जीवन में कुछ बहुत नया हुआ हो। एकदम लीक से हटकर। मैं अंदर जाकर रोटी खाती। टीवी चलाती। दूरदर्शन पर उस समय कश्मकश ज़िंदगी की चलता था। साहिल, तान्या, मयंक… धुंधले से नाम याद हैं।खाना खाकर वापिस उसी रोमांचक रास्ते से मैं वापिस जाती। राजू ताऊ की पत्नी बहुत सारे गीत जानती थीं। वो गुनगुनाने लगतीं तो माँ भी साथ देतीं। माँ मुझे आंखों के इशारे से स्कूल चले जाने को कहतीं। मैं थोड़ी देर ओर वहाँ खड़े रहकर उस अर्द्धवृत्ताकार पैटर्न को देखना चाहती थी जो दीवार लीपते हुए बनता था। पर आधी छुट्टी का समय बहुत जल्दी बीतता था। बीतता नहीं, भागता था। रविवार की रंगोली इन दिनों अस्त व्यस्त रहती। टीवी समेत सारा सामान कमरों से बाहर निकल चुका होता। कमरों के अंदर चिकनी मिट्टी घोलकर बनी दोलक पोती जाती। इससे दीवारें चिकनी हो जाती थीं। मां इसे एक कपड़े से लीपती थीं। मेरा मन होता मैं भी कोशिश करके देखूं।माँ कहतीं कि हाथ फट जायेंगे। बड़ी हो जाओ तब लीप लेना।मैं पास खड़ी रहकर उन्हें देखती रहती। बाबा इन दिनों सारी चारपाइयों की दावण कसने का काम बड़े नियम से कर रहे होते थे। दादी भी उनका साथ देतीं। पापा ट्रैक्टर से लेकर हल तक सारे संज साधनों को साफ़ करते। जिन पर ज़रूरत होती उन पर रंग करते। उन दिनों की रोनक ही कुछ और थी।मैं जब मां को देखते देखते थक जाती, कमरों से बाहर निकले सामान में कुछ खोजने लगती। हर साल कुछ न कुछ नया खिलौना मिल ही जाता था। वो खिलौना नहीं होता था, कोई चीज़ होती थी जिसके लिए मां के देतीं कि अब काम की नहीं, खेलने को ले लो। एक साल पुरानी बोतलों से बनी चिमनियां मिलीं, अगले साल हरे रंग वाली लालटेन, फिर रेडियो, उससे अगले साल कैसेट्स मिलीं, उससे अगले साल डेक भी मिल गया। हर साल मेरे खिलौने बढ़ते जा रहे थे। मुझे खुश होना चाहिए था। खेलने में खो जाना चाहिए था। पर पता नहीं क्यों मुझे वो सारा सामान जो अलमारियों में सजा रहता था, उसे यूं पड़ा देखकर उदासी महसूस होती।मां कमरों के बाहर कली करने पर पहुंच जाती। कली में रंगत लाने के लिए थोड़ी सी सूखी नील चूने वाली हांडी में मिलाई जाती। पहला ब्रश दीवार पर फिरता और खुशबू! देखते ही देखते पूरा घर सुंदर बन जाता। एकदम नया। हल्की नीली आभा वाले बगुले जैसा। और मैं सारी नई चीज़ों के पुराने हो जाने का दुःख भूल जाती। दिवाली के दियों को परात में भिगोकर तैयार करना, बाती बनाना, गोवर्धन पूजा के लिए बाबा के साथ जाकर बाजरी का सिट्टा और काचर खोजकर लाना, और भी कई तरह के कामों की सूची मन में बनने लगती जिसका उत्साह रहता। मुझे उस उत्साह की सबसे ज़्यादा याद आती है। त्योहार त्योहार जैसा नहीं लगता, वो खुशबू कहां है? वो नील के खाली डिब्बे जिनसे खेलते हुए रंग मेरे हाथ नीले हो जाते थे। मैं सोचती थी दीवार ज़्यादा सुंदर या मेरे हाथ? माँ के हाथ फट जाते थे। पर वो खुश रहतीं। घर की सफ़ाई इतने अच्छे से हो जाना उन्हें शुभ लगता। अब अच्छा ही है ना कि शुभ के लिए इतनी मेहनत नहीं लगती। पर तब भी मां अक्सर उन दिनों की बात कर लेती हैं। उस दूसरे गांव की बात कर लेती हैं जो बहुत दूर छूट गया।हमारे पूरे पक्के घर के पिछले हिस्से में एक छोटा सा आंगन उन्होंने अब भी बचा रखा है। उसे हर साल अकेले ही गोबर से लीपती हैं और राजू ताऊ की पत्नी से सीखे गीत गुनगुनाती हैं। मैं चाय बनाकर उनके पास ले जाती हूं। हम साथ में चाय पीते हैं। मां अपनी सहेलियों की बातें करती हैं। मां उस पीछे छूटे गाँव की बातें करती हैं। मैं सुनती और सोचती हूं कि क्या सच में वो गाँव कहीं छूटा है? बचा है? शायद नहीं। वो गांव, वो त्योहार, वो लोग, वो तैयारियां सब किसी ने झोले में भरे और बच्चे को दे दिए – अब ये काम के नहीं। तुम इनसे खेल सकते हो।वो बच्चा समय था। हमारी सारी स्मृतियां अब उसके खिलौनों में रखी हैं। उसे कोई दुःख भी नहीं। बिल्कुल भी नहीं। वो हमें बीतते के साथ रीतता देखता है, छटपटाता देखता है। हँसता और कह देता है – त्योहार शुभ हो। त्योहार शुभ हो!
दीक्षा चौधरी